
समाज का सबसे गहरा संकट तब जन्म लेता है, जब उसकी सबसे मूल इकाई - परिवार अपने ध्येय और दायित्व को विस्मृत करने लगती है। आज यह स्थिति हमें समाज में दृष्टिगोचर हो रही है। भारतीय जीवन-दृष्टि में परिवार केवल एक सामाजिक संरचना मात्र नहीं है, वरन् वह एक जीवंत, स्पन्दनशील और आध्यात्मिक संस्था के रूप में स्थापित रहा है। पर आज जिस गति से परिवार की धुरी अपने अक्ष से डिग रही है, वह केवल सामाजिक संकट नहीं, सांस्कृतिक अवसाद है।
आधुनिकता की आंधी ने जहाँ अधिकारों और स्वतंत्रता की भाषा को स्वर दिया, वहीं उत्तरदायित्व और सह-अस्तित्व जैसे मौलिक तत्व चुपचाप नेपथ्य में चले गए हैं। इस विस्थापन का सर्वाधिक मार्मिक प्रभाव उस पीढ़ी पर पड़ा है जिसने परिवार की अवधारणा को निष्ठा, समर्पण और परंपरा से सींचा है।
पहले बेटे का विवाह घर में उत्सव का वातावरण रच देता था- माता पिता के मन में नई आशा और सुरक्षित भविष्य की रोशनी भर देता था। अब स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। आज पुत्र का विवाह माता पिता के मन में आशंका, भय और असुरक्षा भाव लेकर आता है। कई माता-पिताओं के लिए तो अघोषित संकटकाल तक बन जाता है। यह बदलाव केवल माता-पिता की स्थिति में ही नहीं आया है बेटा भी उतना ही प्रभावित हुआ है।
विवाहोपरांत जब बेटा पत्नी के साथ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में खड़ा होता है, तो यह स्वाभाविक सामाजिक विकास प्रतीत होता है। किंतु जब उस इकाई के घेरे उसके लिए अपने मूल परिवार के प्रति एक उदासीनता, संकोच या परोक्ष अपराधबोध का कारण बनने लगते हैं, तो यह एक गहरे आंतरिक द्वंद्व का संकेत बन जाता है।
यह द्वंद्व अकेले बेटे का या अकेले माता पिता का नहीं होता, दोनों ही इसमें पिसते हैं। पुत्र एक ओर तो अपने जीवनसाथी की अपेक्षाओं और ससुराल पक्ष की अघोषित निगरानी के नीचे होता है और दूसरी तरफ माता-पिता की मौन आकांक्षाओं और स्नेह की स्मृतियों से जकड़ा होता है। इस दोहरे संघर्ष में फंसा उसका मन असमर्थता को चुप्पी में ढाल लेता है, और वह चुप्पी धीरे-धीरे रिश्तों के दरवाज़े बंद कर देती है। कई प्रकरण में हमने इसे आत्महत्या बनते भी देखा है।
माता-पिता अपना बेटा सुखी रहे और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे के भाव से चालित बहू से मिलने वाली अवमानना और उपेक्षा का कड़वा घूंट पीकर जीने की विवशता को स्वीकार कर लेते हैं। तनाव और दुःख के कारण अनेक बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाते हैं, पर किसी से कुछ कहते नहीं।
इसी तारतम्य में हम यदि आज के विधिक परिदृश्य को देखते हैं तो वह पूरी लड़की के पक्ष में है तथा पुरुष और उसके परिवार के लिए उत्पीड़न के जोखिम से भरा है। जिस समाज ने वर्षों तक स्त्री को दबाया था, वही समाज अब क्षतिपूर्ति की ऐसी प्रवृत्तियों में उलझ गया है। वह पुनर्संतुलन की जगह एक नया असंतुलन जन्म दे चुका है। यह भय कि कोई भी बात शिकायत बन सकती है, और कोई भी मतभेद अपराध की श्रेणी में आ सकता है - यह एक मनोवैज्ञानिक असुरक्षा का भयावह संकेत बन गया है। इससे न केवल रिश्तों में संदेह आया है, बल्कि परिवार की सहजता, संवाद और आपसी विश्वास का क्षरण हो रहा है।
लड़की के माता-पिता जब अपनी बेटी के विवाहित जीवन में निरंतर उपस्थिति बनाए रखते हैं, तो यह ‘संरक्षण’ के नाम पर एक गुप्त आक्रामकता का रूप ले लेता है। यह आक्रामकता बेटी को तो यह विश्वास देती है कि वह सही है, भले ही उसकी दृष्टि कितनी ही सीमित, विकृत या स्वार्थ ग्रस्त हो। इसके विपरीत यह भाव लड़के के आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर क्षीण करता है। धीरे-धीरे वह एक आत्म-संदेह की स्थिति में पहुँचता है - जहाँ न वह अपने निर्णयों पर भरोसा कर पाता है, न अपनी भावनाओं पर। यह आत्म-संदेह, मनोवैज्ञानिक रूप से एक व्यक्ति को निष्क्रिय, तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त बनाता है। इन स्थितियों का सबसे गहरा, आघात होता है उन पर जिन्हें हमने 'वरिष्ठ नागरिक' कहकर सम्मानित तो किया, पर व्यावहारिक जीवन में उन्हें जीवन की देहरी पर अकेला छोड़ दिया।
वृद्धावस्था, जो भारतीय परंपरा में अनुभव, आशीर्वाद और मार्गदर्शन का काल था, आज एक मौन निर्वासन में परिवर्तित हो गया है। जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष संतान की परवरिश में लगाए, वे अब दरकिनार कर दिए गए हैं - ना शिकायत कर सकते हैं, ना समीप आ सकते हैं। उनकी पीड़ा एक ‘अस्वीकृत प्रेम’ की तरह है - यह उन्हें भीतर से तोड़ देती है। कई वृद्ध इस अस्वीकार्यता को मनोवैज्ञानिक अपमान की तरह झेलते हैं। वे अपने को आत्मसम्मान हीन और अस्तित्वहीन मानने लगते हैं। कुछ के लिए यह दुःख इतना तीव्र होता है कि वे जीवन से मुँह मोड़ने को विवश हो जाते हैं।
यह स्थिति केवल परिवारों के लिए ही नहीं, पूरे समाज के भावात्मक ढाँचे के विघटन की ओर संकेत है। हमारे यहां परिवार वह स्थान होता था जहाँ व्यक्ति स्वयं को बिना शर्त स्वीकृत पाता था, और आज वही स्थान भय, संकोच, अस्वीकार और संघर्ष की भूमि बन गया है—तो यह मात्र सामाजिक संकट नहीं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक शून्य है। इस शून्य को अधिकारों से नहीं, केवल उत्तरदायित्व की पुनर्स्थापना से भरा जा सकता है।
आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम स्त्री-पुरुष के अधिकारों का तुलनात्मक विश्लेषण करें, बल्कि इस बात की है कि हम संबंधों की भाषा को पुनः मानव केंद्रित, भावना केंद्रित और दायित्व-केंद्रित बनाएँ।
वरना आने वाले समय में परिवार केवल एक सामाजिक ढांचा मात्र रह जाएगा, जिसमें न ऊष्मा होगी, न आत्मीयता—सिर्फ एक अनाम विधिक समझौता, जो भीतर से सबको संवेदनहीन और खोखला बना देगा।


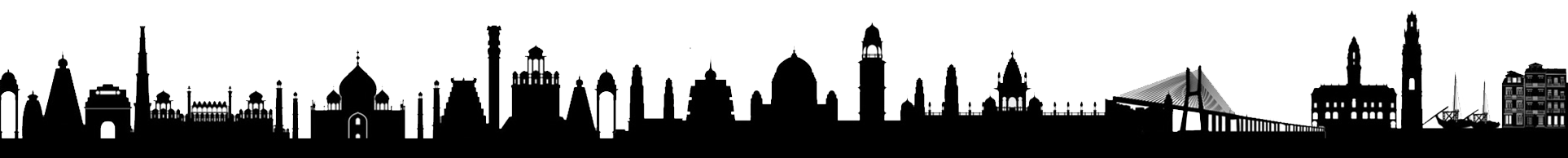
Login to Leave Comment
LoginNo Comments Found
संबंधित आलेख
पूर्णिमा का महत्व | पूर्णिमा व्रत
सप्ताह के किस दिन करें कौन से भगवान की पूजा | सात वार का महत्व
महा मृत्युंजय मंत्र का अर्थ, उत्पत्ति और महत्व | महा मृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय रखें इन बातों का ध्यान | Maha Mrityunjaya Mantra
हिंदी भाषा से जुड़े रोचक तथ्य
मंदिर शब्द की उत्पत्ति कब हुई | मंदिर का निर्माण कब से शुरू हुआ?
तुलसी जी कौन थी? कैसे बनी तुलसी पौधे के रूप में ? | तुलसी विवाह
हिंदी वर्णमाला की संपूर्ण जानकारी | हिंदी वर्णमाला
अच्युत, अनंत और गोविंद महिमा
निष्कामता
हर दिन महिला दिन | Women's Day
33 कोटि देवी देवता
हिंदू संस्कृति के 16 संस्कार
हिंदी दिवस
शिक्षक दिवस
राखी
बचपन की सीख | बच्चों को लौटा दो बचपन
बात प्रेम की
महामाया मंदिर रतनपुर | संभावनाओ का प्रदेश - छत्तीसगढ़ | मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ननिहाल
माँ बमलेश्वरी मंदिर | संभावनाओ का प्रदेश - छत्तीसगढ़
माँ चंद्रहासिनी मंदिर | संभावनाओ का प्रदेश - छत्तीसगढ़
खल्लारी माता मंदिर | संभावनाओ का प्रदेश - छत्तीसगढ़
भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे | भारत देश
विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस | World Menstrual Hygiene Day
ज्योतिष शास्त्र | शनि न्याय प्रिय ग्रह क्यों है ?
वास्तु शास्त्र | वास्तुशास्त्र का उदगम
वास्तुशास्त्र में पूजा कक्ष का महत्व
पंचवटी वाटिका | पंचवटी का महत्व स्कंद पुराण में वर्णित
कृतज्ञता: मानसिक सेहत, रिश्तों और सकारात्मक जीवन का आधार
ज्योतिष की विभिन्न विधाये और राजा सवाई जयसिंह (जयपुर) का योगदान
संस्कारों की प्यारी महक
मिच्छामि दुक्कडम्
सत्संग बड़ा है या तप
ब्रह्मांड के स्वामी शिव
बलिदानी - स्वतंत्रता के नायक
महामृत्युंजय मंत्र | महामृत्युंजय मंत्र जाप
राम राज्य की सोच
भारतीय वैदिक ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय
भारतीय वैदिक ज्योतिष का प्रचलन
मैच बनाने की मूल बातें (विवाह और ज्योतिष)
कुंडली मिलान | विवाह के लिए गुण मिलान क्यों महत्वपूर्ण है?
कुंडली चार्ट में घरों की बुनियादी समझ
सनातन संस्कृति में व्रत और त्योहारों के तथ्य
सनातन संस्कृति में उपवास एवं व्रत का वैज्ञानिक एवं धार्मिक पक्ष
2 जून की रोटी: संघर्ष और जीविका की कहानी
प्रकृति की देन - पौधों में मौजूद है औषधीय गुण
प्री वेडिंग – एक फिज़ूलखर्च
दो जून की रोटी
गणेश जी की आरती
भारतीय परम्परा की प्रथम वर्षगांठ
नव वर्ष
नहीं कर अभिमान रे बंदे
आज का सबक - भारतीय परंपरा
चाहत बस इतनी सी
नारी और समाज
माँ तू ऐसी क्यों हैं...?
दर्द - भावनात्मक रूप
पुरुष - पितृ दिवस
मितव्ययता का मतलब कंजूसी नहीं
सावन गीत
आया सावन
गुरु पूर्णिमा - गुरु की महिमा
सार्वजानिक गणेशोत्सव के प्रणेता लोकमान्य तिलक
शास्त्रीजी की जिन्दगी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है | लाल बहादुर जयंती
कन्याओं को पूजन से अधिक सुरक्षा की जरूरत है ...!
जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है
धर्म - धारण करना
आलस्य (Laziness)
प्रतिष्ठित शिक्षक - प्रेरक प्रसंग
राष्ट्र का सजग प्रहरी और मार्गदृष्टा है, शिक्षक
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?
संस्कृति का उद्गम संस्कृत दिवस | Culture origin in Sanskrit Day
75 बरस की आजादी का अमृत महोत्सव और हम
एक पाती शिक्षक के नाम – शिक्षक की भूमिका और मूल्य आधारित शिक्षा
बच्चों को लौटा दो बचपन – आधुनिक पालन-पोषण पर एक प्रेरक विचार
रामबोला से कालिदास बनने की प्रेरक कथा – भारत के महान कवि की जीवनी
त्रिदेवमय स्वरूप भगवान दत्तात्रेय
गणतंत्र दिवस – 26 जनवरी का इतिहास, महत्व और समारोह
बीते तीन साल बहुत कुछ सीखा गया | 2020 से 2022 तक की सीखी गई सीखें | महामारी के बाद का जीवन
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं | कोविड से बचाव के लिए मजबूत इम्यूनिटी
वैदिक काल की विदुषी : गार्गी और मैत्रेयी
वर्तमान दौर में बदलता प्रेम का स्वरूप – एक विचारणीय लेख
जल संरक्षण आवश्यक है – पानी बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं
कुटुंब को जोड़ते व्रत और त्योहार – भारतीय परंपराओं का उत्सव
मेरे गाँव की परिकल्पना – विकास और विनाश पर एक काव्यात्मक चिंतन
जलवायु परिवर्तन और हमारी जिम्मेदारी: अब तो जागो
राजा राममोहन राय - आधुनिक भारत के जनक | भारत के महान समाज सुधारक
भविष्य अपना क्या है? | तकनीक और मोबाइल लत का युवाओं पर असर
प्रकृति संरक्षण ही जीवन बीमा है – पेड़ बचाएं, पृथ्वी बचाएं
वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान – समान अधिकार और आध्यात्मिक ज्ञान
मेरे पिताजी की साइकिल – आत्मनिर्भरता और सादगी पर प्रेरक लेख
भारत रत्न गुलजारीलाल नन्दा (Guljarilal Nanda) – सिद्धांत, त्याग और ईमानदारी का प्रतीक
डिजिटल उपवास – बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है?
नववर्ष संकल्प से सिद्धि | सकारात्मक सोच, अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति
पीपल की पूजा | भारतीय परंपरा में पीपल पूजा का वैज्ञानिक आधार
जीवन में सत्य, धन और आत्मनियंत्रण की प्रेरणा
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में इसका महत्व
महिला समानता दिवस | नारी सशक्तिकरण: चुनौतियाँ, प्रगति और भविष्य
मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या का महत्व
हिंदी की उपेक्षा अर्थात संस्कृति की उपेक्षा | हिंदी : हमारी भाषा, संस्कृति और शक्ति
चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता
श्रावण माह: त्योहारों की शुरुआत
रिश्वतखोरी का अभिशाप
भारतीय संस्कृति की पहचान
प्रवासी भारतीय ही भारतीय संस्कृति के पहरेदार | नीदरलैंड में भारतीय संस्कृति का उजागर
वेदों की अमूल्य सूक्तियाँ – जानिए 80 अनमोल वैदिक रत्न
उत्सव नीरस जीवन में भरते है रंग | जीवन में उत्सवों का महत्व
सूर्य को जल अर्पण करना | सूर्य नमस्कार
विकसित सोच: सफलता की असली कुंजी
राम – सत्य और धर्म का सार
रावण की हड़ताल: दशहरा विशेष व्यंग्य
नथ का वजन – एक परंपरा का अंत
दुविधा – अनुभव और अस्वीकार्यता के बीच की दूरी
घर की लक्ष्मी हैं गृहणियाँ
आत्मकथा वसंत की | वसंत ऋतु
परीक्षा से डर कैसा
गाय और इस्लाम: विश्वास, नियम और सम्मान
भारतीय नववर्ष बनाम अंग्रेजी नववर्ष
श्रीराम - धर्म के मूर्तिमान स्वरूप
नदियों को बचाएं – जीवन और संस्कृति की रक्षा करें
भगवान श्रीराम के उच्चतम आदर्श
सनातन धर्म और अंधविश्वास का सच
विज्ञान दिवस और हमारे वैज्ञानिक
अमृत महोत्सव में संयम व नैतिकता: राष्ट्र निर्माण की आधारशिला
जीवन में सफलता के लिए निरंतर सीखना जरूरी
राम के आदर्श: रामायण से जीवन सीखें और अपने आचरण में उतारें
बच्चे सीखें भगवान श्रीराम के जीवनादर्श | रामायण से नैतिक शिक्षा
नारी का सम्मान और सामाजिक योगदान
यक्ष और युधिष्ठिर का दिव्य संवाद
राम राज्य का दर्शन और आधार
सफलता की ओर साधना से रास्ता
सोने की सही दिशा कौनसी है? | उत्तर दिशा में सिर करके सोना क्यों वर्जित है?
कठिन समय में कौन साथ है?
माँ के अटूट प्रेम को सलाम
दो जून की रोटी - संघर्ष की कहानी
प्री-वेडिंग शूट: आधुनिकता की अंधी दौड़ या सांस्कृतिक पतन?
स्थानीय व्यापार का समर्थन करें
जीवन का असली उद्देश्य – सेवा, प्रेम और सद्भावना से जीवन जीना
चलते रहने का महत्व – कर्म, धैर्य और सकारात्मक सोच की ताकत
घोड़े पर योद्धा की मूर्तियों के संकेत: मुद्रा क्या दर्शाती है?
मानसिक शांति के लिए क्यों ज़रूरी है एक अच्छी दिनचर्या?
आलस्य और डर से बाहर निकलें: मानसिकता में बदलाव
क्या वास्तव में “बी प्रैक्टिकल” होना ज़रूरी है?
अपराध नियंत्रण में संस्कारों की भूमिका और सामाजिक सुधार
विनम्रता: व्यक्तित्व को निखारने वाला सबसे सुंदर मानवीय गुण
दीपोत्सव: भारतीय व्यापार, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा
राम से बड़ा राम का नाम
सफलता का फार्मूला: अभ्यास और जीवन मूल्य
पर्यावरण संकट बढ़ रहा है—अब बदलाव हमारी ज़िम्मेदारी है
अन्न का दुरुपयोग – दिखावे की संस्कृति में बर्बादी
किशोरों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियाँ
अयोध्या राम मंदिर का इतिहास और निर्माण
पहलगाम हमला: जब इंसानियत को धर्म से तोला गया
श्रम बिकता है, बोलो... खरीदोगे?
जीवन में सफलता के लिए धैर्य का महत्व
अहंकार का अंधकार | व्यक्तित्व और समाज पर प्रभाव
चलिष्याम निरंतर | जोखिम, परिवर्तन और सफलता का संबंध
रामायण महाभारत के युद्ध बनाम आधुनिक युद्ध
सच कहने का साहस है.. सलीका है कविता
सामाजिक संकट एवं सांस्कृतिक अवसाद की ओर बढ़ते भारतीय परिवार
चातुर्मास - सनातनी विज्ञान | पाँच तत्व, विज्ञान और परंपरा
मानवीय सद्गुण की आज बड़ी जरूरत | विनम्रता की शक्ति
जीवन में निर्णय का महत्व
तुलसीदास की दृष्टि में नारी शक्ति, प्रकृति, अग्नि और काल का दर्शन
प्रदूषण और निजी वाहनों का बढ़ता प्रभाव
सरकारी नियंत्रण से मन्दिरों को मुक्त करें – एक सनातनी पुकार
खिचड़ी: ढाई हजार साल पुराना भारतीय व्यंजन, स्वाद, परंपरा और इतिहास के साथ
भारत के शहरी क्षेत्रों में वाहन पार्किंग की चुनौतियाँ और समाधान
सहनशीलता का गिरता स्तर और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव | धैर्य और क्षमा का महत्व
कुंबकोणम के शक्ति मुत्तम मंदिर और गरीब पंडित की बगुला संदेश की कहानी
क्या हमारे कार्य करने की कोई सीमा होती है?
कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और अपनी असली क्षमता पहचानें
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – नारी शक्ति को सलाम
शब्द ही ब्रह्म है क्योंकि शब्दों से ही इस त्रिगुणात्मक संसार का सृजन संभव है
आंतरिक और बाहरी दुनिया — ध्यान से आत्म नियंत्रण की शक्ति
हेमू कालाणी – भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानी
नए वर्ष का स्वागत: सकारात्मक विचार, संकल्प और जीवन को खुशहाल बनाने वाले मंत्र
21वीं सदी: अवसर, चुनौतियाँ और डिजिटल युग में बाल मन का भविष्य
दर्शन क्या है? देखने और दर्शन के गहरे अंतर की आध्यात्मिक समझ
भक्ति का सच्चा अर्थ: मंदिरों से आगे, मानवता की ओर
क्षमा का मूल्य: भारतीय संस्कृति में क्षमाशीलता की परंपरा
अज्ञान से ज्ञान की ओर: वैदिक साहित्य में प्रकाश, सद्गुण और श्रेय मार्ग का संदेश
नारी: परिवार की कुशल प्रबंधक — भारतीय संस्कृति में नारी की शक्ति, भूमिका और महत्व
जीवन की बाँसुरी: सरलता से चुनौतियों को मधुर बनाने की कला
उत्तर भारत में पराली जलाना: किसानों और पर्यावरण के लिए स्थायी समाधान
पहली तूलिका, पहली कहानी: भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का अद्भुत संसार
रामचरितमानस में हास्य और व्यंग्य: तुलसीदास की अनोखी रचनात्मकता
भाषा का महत्व: मधुर वाणी, संस्कार और सभ्यता का वास्तविक परिचय
जीवन की बाँसुरी: कठिनाइयों को सरलता से जीतने की प्रेरणादायक सीख
हर विचार का आकर्षण
भारतीय नववर्ष क्यों मनाया जाता है??
डॉ. विक्रम साराभाई: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक
वीर बाल दिवस 26 दिसंबर | साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की अमर शहादत
माँ सरस्वती की आरती | विद्या की देवी
2026: समय की देहरी पर जागरण का वर्ष | चेतना, समाज और राष्ट्र पर विचार
मानव जीवन का दर्शन: धैर्य, समत्व और अनुभव की सनातन दृष्टि
अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय: आज की आवश्यकता | भारतीय दृष्टि
लोकतंत्र और भारतीय ज्ञान परंपरा | वैदिक जड़ें, संविधान और आधुनिक भारत
स्वामी दयानन्द सरस्वती: आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक और ऋषि
प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा एवं संस्कृत कथा साहित्य – दर्शन, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत
धर्म और कर्म का सच्चा अर्थ – कर्तव्य, निष्काम कर्म और जीवन का उद्देश्य
संवाद संस्कृति और बाल मनोविज्ञान – बच्चों को गलत निर्णय और आत्महत्या से कैसे बचाएं
बसंत ऋतु में होली – फागुन, प्रकृति और रंगों के उत्सव का मनोहारी वर्णन
मां लक्ष्मी आरती – संपूर्ण लक्ष्मी जी की आरती
माँ पार्वती आरती – संपूर्ण आरती
लेखक के अन्य आलेख
अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय: आज की आवश्यकता | भारतीय दृष्टि
सामाजिक संकट एवं सांस्कृतिक अवसाद की ओर बढ़ते भारतीय परिवार
डोम्लुर का सूर्य नारायण मंदिर – परंपरा और परिवार भाव को संजोता जीवंत मंदिर
दक्षिणेश्वर काली मंदिर: आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक शक्ति की कहानी
ओरछा: रामराजा की नगरी | आध्यात्मिक यात्रा और सांस्कृतिक विरासत
भक्ति, शक्ति और सौंदर्य की त्रिवेणी : कामाख्या देवालय