
सहनशीलता का गिरता स्तर
सहनशीलता का गिरता स्तर- समाज के लिए हानिकर
आज भौतिकतावाद, एकाकी परिवार और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में सहनशीलता शनैः शनैः क्षीण होती जा रही है। है। इस समस्या के मूल में मूल्यों की अवमानना/ स्वार्थपरता की बढ़ती प्रवृत्ति/माता-पिता द्वारा उचित देखरेख में कमी/बुजुर्गों के सान्निध्य का अभाव आदि कारणों से इंकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ज़रा-ज़रा सी बात पर व्यक्ति अपना आपा खो देता है। तनिक से आवेश में ही बात लड़ाई- झगड़े व मार- पीट तक पहुँच जाती है। छोटी सी बात को भी सहन न करने के कारण दाम्पत्य जीवन में खटास बढ़ रही है। समाज पारिवारिक विखण्डन के दंश को झेलने के लिए विवश है। पारस्परिक संबंध वैमनस्य का सामना कऱ रहे हैं। रिश्ते-नातेदारी में दूरियाँ बढ़ रही हैं। पास-पड़ोस में अपनत्व क्षीण हो रहा हैं। उल्लेखनीय है कि सामान्य से प्रकरण में भी क्रोधित हो जाना और असहनशीलता का परिचयदेना वैयक्तिक/सामाजिक स्वास्थ्य को चिह्नित करता है।
सहनशीलता का गिरता ग्राफ प्रबुद्धजनों के लिए चिंतनीय संदर्भ बनता जा रहा है। इसमें कोई संशय नहीं कि वैश्विक स्तर पर भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। ‘असहनशीलता’ के संभावित नकारात्मक प्रभाव से दूर रहने के लिए संचेतना आवश्यक है। निस्संदेह, आज के दौर में सामाजिक उत्कर्ष के निमित्त विचारों में सहनशीलता को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण दिखाई देता है।
‘मनुष्यता’ की अभिव्यक्ति में सहायक है सहनशीलता। इससे व्यक्ति की सौम्य प्रकृति उद्घाटित होती है। इसमें ‘‘जियो और जीने दो’’ का आदर्श समाहित है। यह न तो किसी से सहमति है और न ही अन्याय के समक्ष तटस्थता। वस्तुतः यह तत्व मानवता के प्रति सम्मान है। निहित स्वार्थ और संकुचित सोच के ज्ञापक दूषित विचारों के विरुद्ध शांत प्रतिक्रिया है। यह संयमन का प्रकटीकरण है। सामाजिक ताने-बाने की मजबूती के लिए व्यावहारिक स्तर पर लचीलेपन की प्रस्तुति है। यह सामाजिक विखण्डन को रोकता है। सहन-शक्ति का आश्रय लेकर व्यक्ति/ परिवार/समाज में अनुकूलता का समावेश असंभव नहीं।
सहनशीलता परिवेश में सकारात्मकता को प्रसारित करने में सहायक है। आर्ष मार्गदर्शन है कि दुष्ट प्रकृति वाले लोगों के अनर्गल बातों को सहन करना तथा श्रेष्ठ लोगों के सदाचरण में सदा संलग्न रहना ही समीचीन है-
सद्भिः पुरुस्तादभिपूजितः स्यात् सद्भिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्यात्।
सदासतामतिवादांस्तितिक्षेत् सतां वृत्तं चाददीतार्यवृत्तः।। महाभारत/आदि पर्व/अध्याय 87/श्लोक 10
सहनशीलता एक सांस्कृतिक विचारणा है जिससे समाज में व्यक्ति की संस्थिति निर्मित होती है। सामाजिक सौहार्द को विस्तारित करने में सहनशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके सुप्रभाव में प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भी अनुकूलता की संभावना निहित है। यह सद्गुण उग्रता को शांत करता है है। वस्तुतः किसी के विचार/व्यवहार को असहमति के पश्चात् भी सहजता से सहन कर लेना स्वयं में शांति का आधार बनता है। इस तरह सहनशीलता की कथित उपलब्धि सामान्य तो नहीं।
यह वैशिष्ट्य मानव संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का प्रकटीकरण करता है। जटिल स्थितियों को संभालने का सामर्थ्य रखता है। विसंगतियों को सुसंगत बनाता है। सह-अस्तित्व में सहायता करता है। सामाजिकों में आत्मीयता को बढ़ावा देता है। आत्मनियंत्रण में सहायता करता है। परिवार, रिश्तेदार, मित्र, पास-पड़ोस में सामंजस्य बढ़ाता है। इस तरह परिवेश में शांति-सद्भाव-सौहार्द को प्राथमिकता देता है। संवेदनात्मक दृष्टिकोण रखने के कारण मानवता के संरक्षण में प्रभावकारी है। निस्संदेह, सामाजिक स्वरूप में रचनात्मक परिवर्तन की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रयोजनीय कहना उपयुक्त है।
समाज में व्याप्त विसंगतियों से सामना होना तो जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु सहनशीलता का सहारा लेकर बहुविध जटिलताओं को सुलझाना- चुनौतियों का सामना करना- द्वेष विद्वेष का परिहार करना जीवन का सौंदर्य है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव जीवन में व्यष्टि व समष्टि स्तर पर अच्छे संबंधों की आवश्यकता होती है और सहनशीलता इसमें कारगर है। यह मनुष्य के लिए आभूषणवत् है जो उसकी सामाजिक संस्थिति को निर्मित करती है। संसार यात्रा को सुगम बनाता है सहनशीलता का आश्रय। धैर्य और संयम को बढ़ावा मिलता है इससे। व्यक्तित्व को विनम्र बनाकर समाज के संस्करण व परिष्करण की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।
सहिष्णुता, क्षान्ति, तितिक्षा सहनशीलता के ही अपर पर्याय हैं।
सनातन संस्कृति से हस्तगत यह अवधारणा का मानवता के संरक्षण में योगदान देती है। जटिल परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सहनशीलता महत्वपूर्ण भूमिका रचती है। हां, यह अवश्य है कि सहनशील व्यक्ति में शांति और संतोष का व्यापन एक स्वाभाविक उपलब्धि है। यह वैचारिक संघर्ष को रोक सकती है। तनाव को दूर कर सकती है। सहनशीलता एक शक्ति है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आने वाले उतार- चढ़ाव का सामना करने में सहयोग करती है।
वर्तमान में ’’सहिष्णुता’’ शब्द का कुछ अर्थभेद के साथ तात्पर्य है- दूसरों के कार्यों और विचारों के प्रति उदार भावना रखना। सहनशीलता के सुप्रभाव में व्यक्ति दूसरों के विचार-विश्वास-व्यवहार के प्रति सम्मान का भाव रखता है। यह व्यक्ति को उग्र प्रतिक्रिया से विरत करता है। सहनशीलता आपसी व्यवहार में विनम्रता को संरक्षित करती है।
‘क्षान्ति’ शब्द सहनशीलता के लिए प्रयुक्त होता है। सामर्थ्यवान होते हुए भी अपराधी के प्रति किसी भी प्रकार का दण्ड का भाव न रखना ही क्षान्ति है। श्रीमद्भगवद्गीता में उल्लिखित है कि-
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः।।श्रीमद्भगवद्गीता/13/7
क्षान्ति सह-अस्तित्व में भी मददगार है।
‘‘तितिक्षा’’ मन की एक वृत्ति है। इसका तात्पर्य है- परापराधसहनम् (दूसरों का अपराध सहन करना) इसकी विद्यमानता को विशिष्टता के रूप में स्वीकार किया गया। महर्षि व्यास का स्पष्ट अभिमत है कि-
अक्रोधनो क्रोधनेभ्यो विशिष्टस्तथा तितिक्षुरतितिक्षोर्विशिष्टः।
अमानुषेभ्यो मानुषाश्च प्रधानाः विद्वांस्तथैवाविदुषः प्रधानः।। महाभारत/आदि पर्व/अध्याय 87/श्लोक 6
अनेक दुर्गुणों में ‘अतितिक्षा’ (सहनशीलता का अभाव) का भी उल्लेख किया गया। इन पर नियंत्रण पाने के लिए विवेक की- संयम की- नीति की जरूरत होती है। किंतु जब गुणों से युति बन जाती है तो वह व्यक्ति सामान्य मनुष्य की तुलना में ‘विशेष’ (उत्कृष्ट) माना जाता है। जीवन की श्रेष्ठता में गुणों की अनिवार्यता से इंकार नहीं किया जा सकता। निश्चय ही विवेकी जन इस सद्गुण की महत्ता को अंगीकार कर जीवन को सरल बनाते हैं।
सहनशक्ति में आक्रोश/आवेश को नियंत्रित करने की योग्यता है। प्रायः देखा जाता है कि जब दूसरा पक्ष किसी कटुता को सहन कर लेता है तो अपराध करने वाला पक्ष असफल होने का दंश झेलता है। सद्ग्रंथ असहनशीलता के अवांछित प्रभाव से सचेत करते हैं कि-
आक्रुष्यमानो नाक्रोशेनमन्युरेव तितिक्षतः।
आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति।। महाभारत/आदि पर्व/अध्याय 87/श्लोक 7
यहां सहनशीलता को अपनाना विहित है। ‘मनुष्यता’ के नाते किसी की निंदा- अपशब्दों की प्रतिक्रिया निंदा- अपशब्दों से करना समीचीन नहीं। ऐसे वाग्वाण हृदय को आघात पहुंचाते हैं। दुष्ट जनों के मुख से निःसृत सदोष वचन शोक के कारक बन जाते हैं। अतः विवेकी पुरुष द्वारा दूसरे के प्रति ऐसी वाणी व व्यवहार से विरत रहना तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर सद्व्यवहार करना श्रेयस्कारी है।
कथित स्थिति में सहनशीलता अपनाने से आचार व व्यवहार में आने वाली बाधाओं में कमी देखी जाती है। पूर्वोक्त श्लोक में कहा गया कि यदि शब्दों के द्वारा आक्रोशित किया जा रहा हो तो उसको सहन कर लेना चाहिए, ऐसा करना आक्रोश पैदा करने वाले को ही जला डालता है। ध्यातव्य है कि महात्मा बुद्ध तथा महर्षि दयानन्द के जीवन की अनेक घटनाओं ने उक्त संदर्भ को सुपुष्ट किया है। सहनशीलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है- क्रोध। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति अभावात्मक सोच से मुक्त नहीं हो पाता, इस कारण मन-मस्तिष्क का दुःख-तनाव-विरोध-उग्रता आदि से आच्छादित होना अचम्भे की बात नहीं। कथित आवेग को विलम्बित कर इस पर नियंत्रण में कुछ सीमा तक सफलता पाई जा सकती है। असहनशीलता एक नकारात्मक वृत्ति है, इसके बिना कई बार व्यक्ति बेचैनी को जीता है। कभी-कभी इस वजह से मन व शरीर के लिए कष्टकारी स्थिति निर्मित हो जाती है। सामाजिक पर्यावरण में सुधार की दृष्टि से विचारों में सहनशीलता को प्रश्रय देना सामयिक आवश्यकता है।
सत्संगति- सद्विचार- सद्भावना आदि के माध्यम से सहनशीलता की दिशा प्रशस्त होती है। सामाजिक परिवेश के स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे सशक्त साधन कहना अत्युक्ति नहीं। संदर्भित जागरूकता से सामाजिक स्वरूप को बेहतर बनाने के प्रयासों की अपेक्षा है। नवागत पीढ़ी को सहनशीलता की महत्ता से अवगत कराना उचित है। व्यक्ति/ समाज में रचनात्मक बदलाव के लिए सहनशीलता की व्यावहारिक रूप आवश्यक है। ध्यातव्य है कि सहनशीलता की कमी समाज की एकता में अवरोध डाल सकती है। अन्ततः समाज/राष्ट्र के समुज्ज्वल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की पूर्णता के निमित्त भी इस ओर ध्यान देना युक्तियुक्त है।
लेखक - प्रो. कनक रानी जी


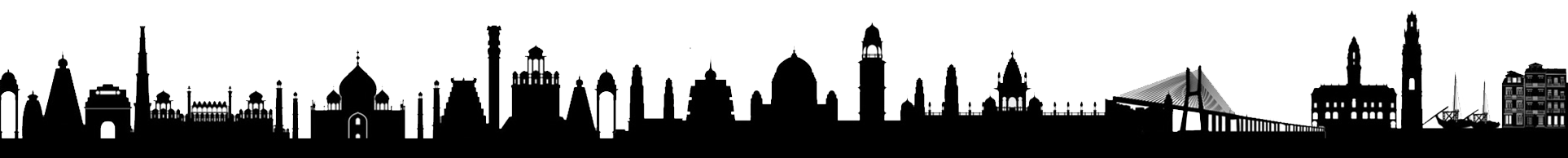
Login to Leave Comment
LoginNo Comments Found
संबंधित आलेख
पूर्णिमा का महत्व | पूर्णिमा व्रत
सप्ताह के किस दिन करें कौन से भगवान की पूजा | सात वार का महत्व
महा मृत्युंजय मंत्र का अर्थ, उत्पत्ति और महत्व | महा मृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय रखें इन बातों का ध्यान | Maha Mrityunjaya Mantra
हिंदी भाषा से जुड़े रोचक तथ्य
मंदिर शब्द की उत्पत्ति कब हुई | मंदिर का निर्माण कब से शुरू हुआ?
तुलसी जी कौन थी? कैसे बनी तुलसी पौधे के रूप में ? | तुलसी विवाह
हिंदी वर्णमाला की संपूर्ण जानकारी | हिंदी वर्णमाला
अच्युत, अनंत और गोविंद महिमा
निष्कामता
हर दिन महिला दिन | Women's Day
33 कोटि देवी देवता
हिंदू संस्कृति के 16 संस्कार
हिंदी दिवस
शिक्षक दिवस
राखी
बचपन की सीख | बच्चों को लौटा दो बचपन
बात प्रेम की
महामाया मंदिर रतनपुर | संभावनाओ का प्रदेश - छत्तीसगढ़ | मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ननिहाल
माँ बमलेश्वरी मंदिर | संभावनाओ का प्रदेश - छत्तीसगढ़
माँ चंद्रहासिनी मंदिर | संभावनाओ का प्रदेश - छत्तीसगढ़
खल्लारी माता मंदिर | संभावनाओ का प्रदेश - छत्तीसगढ़
भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे | भारत देश
विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस | World Menstrual Hygiene Day
ज्योतिष शास्त्र | शनि न्याय प्रिय ग्रह क्यों है ?
वास्तु शास्त्र | वास्तुशास्त्र का उदगम
वास्तुशास्त्र में पूजा कक्ष का महत्व
पंचवटी वाटिका | पंचवटी का महत्व स्कंद पुराण में वर्णित
कृतज्ञता: मानसिक सेहत, रिश्तों और सकारात्मक जीवन का आधार
ज्योतिष की विभिन्न विधाये और राजा सवाई जयसिंह (जयपुर) का योगदान
संस्कारों की प्यारी महक
मिच्छामि दुक्कडम्
सत्संग बड़ा है या तप
ब्रह्मांड के स्वामी शिव
बलिदानी - स्वतंत्रता के नायक
महामृत्युंजय मंत्र | महामृत्युंजय मंत्र जाप
राम राज्य की सोच
भारतीय वैदिक ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय
भारतीय वैदिक ज्योतिष का प्रचलन
मैच बनाने की मूल बातें (विवाह और ज्योतिष)
कुंडली मिलान | विवाह के लिए गुण मिलान क्यों महत्वपूर्ण है?
कुंडली चार्ट में घरों की बुनियादी समझ
सनातन संस्कृति में व्रत और त्योहारों के तथ्य
सनातन संस्कृति में उपवास एवं व्रत का वैज्ञानिक एवं धार्मिक पक्ष
2 जून की रोटी: संघर्ष और जीविका की कहानी
प्रकृति की देन - पौधों में मौजूद है औषधीय गुण
प्री वेडिंग – एक फिज़ूलखर्च
दो जून की रोटी
गणेश जी की आरती
भारतीय परम्परा की प्रथम वर्षगांठ
नव वर्ष
नहीं कर अभिमान रे बंदे
आज का सबक - भारतीय परंपरा
चाहत बस इतनी सी
नारी और समाज
माँ तू ऐसी क्यों हैं...?
दर्द - भावनात्मक रूप
पुरुष - पितृ दिवस
मितव्ययता का मतलब कंजूसी नहीं
सावन गीत
आया सावन
गुरु पूर्णिमा - गुरु की महिमा
सार्वजानिक गणेशोत्सव के प्रणेता लोकमान्य तिलक
शास्त्रीजी की जिन्दगी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है | लाल बहादुर जयंती
कन्याओं को पूजन से अधिक सुरक्षा की जरूरत है ...!
जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है
धर्म - धारण करना
आलस्य (Laziness)
प्रतिष्ठित शिक्षक - प्रेरक प्रसंग
राष्ट्र का सजग प्रहरी और मार्गदृष्टा है, शिक्षक
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?
संस्कृति का उद्गम संस्कृत दिवस | Culture origin in Sanskrit Day
75 बरस की आजादी का अमृत महोत्सव और हम
एक पाती शिक्षक के नाम – शिक्षक की भूमिका और मूल्य आधारित शिक्षा
बच्चों को लौटा दो बचपन – आधुनिक पालन-पोषण पर एक प्रेरक विचार
रामबोला से कालिदास बनने की प्रेरक कथा – भारत के महान कवि की जीवनी
त्रिदेवमय स्वरूप भगवान दत्तात्रेय
गणतंत्र दिवस – 26 जनवरी का इतिहास, महत्व और समारोह
बीते तीन साल बहुत कुछ सीखा गया | 2020 से 2022 तक की सीखी गई सीखें | महामारी के बाद का जीवन
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं | कोविड से बचाव के लिए मजबूत इम्यूनिटी
वैदिक काल की विदुषी : गार्गी और मैत्रेयी
वर्तमान दौर में बदलता प्रेम का स्वरूप – एक विचारणीय लेख
जल संरक्षण आवश्यक है – पानी बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं
कुटुंब को जोड़ते व्रत और त्योहार – भारतीय परंपराओं का उत्सव
मेरे गाँव की परिकल्पना – विकास और विनाश पर एक काव्यात्मक चिंतन
जलवायु परिवर्तन और हमारी जिम्मेदारी: अब तो जागो
राजा राममोहन राय - आधुनिक भारत के जनक | भारत के महान समाज सुधारक
भविष्य अपना क्या है? | तकनीक और मोबाइल लत का युवाओं पर असर
प्रकृति संरक्षण ही जीवन बीमा है – पेड़ बचाएं, पृथ्वी बचाएं
वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान – समान अधिकार और आध्यात्मिक ज्ञान
मेरे पिताजी की साइकिल – आत्मनिर्भरता और सादगी पर प्रेरक लेख
भारत रत्न गुलजारीलाल नन्दा (Guljarilal Nanda) – सिद्धांत, त्याग और ईमानदारी का प्रतीक
डिजिटल उपवास – बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है?
नववर्ष संकल्प से सिद्धि | सकारात्मक सोच, अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति
पीपल की पूजा | भारतीय परंपरा में पीपल पूजा का वैज्ञानिक आधार
जीवन में सत्य, धन और आत्मनियंत्रण की प्रेरणा
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में इसका महत्व
महिला समानता दिवस | नारी सशक्तिकरण: चुनौतियाँ, प्रगति और भविष्य
मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या का महत्व
हिंदी की उपेक्षा अर्थात संस्कृति की उपेक्षा | हिंदी : हमारी भाषा, संस्कृति और शक्ति
चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता
श्रावण माह: त्योहारों की शुरुआत
रिश्वतखोरी का अभिशाप
भारतीय संस्कृति की पहचान
प्रवासी भारतीय ही भारतीय संस्कृति के पहरेदार | नीदरलैंड में भारतीय संस्कृति का उजागर
वेदों की अमूल्य सूक्तियाँ – जानिए 80 अनमोल वैदिक रत्न
उत्सव नीरस जीवन में भरते है रंग | जीवन में उत्सवों का महत्व
सूर्य को जल अर्पण करना | सूर्य नमस्कार
विकसित सोच: सफलता की असली कुंजी
राम – सत्य और धर्म का सार
रावण की हड़ताल: दशहरा विशेष व्यंग्य
नथ का वजन – एक परंपरा का अंत
दुविधा – अनुभव और अस्वीकार्यता के बीच की दूरी
घर की लक्ष्मी हैं गृहणियाँ
आत्मकथा वसंत की | वसंत ऋतु
परीक्षा से डर कैसा
गाय और इस्लाम: विश्वास, नियम और सम्मान
भारतीय नववर्ष बनाम अंग्रेजी नववर्ष
श्रीराम - धर्म के मूर्तिमान स्वरूप
नदियों को बचाएं – जीवन और संस्कृति की रक्षा करें
भगवान श्रीराम के उच्चतम आदर्श
सनातन धर्म और अंधविश्वास का सच
विज्ञान दिवस और हमारे वैज्ञानिक
अमृत महोत्सव में संयम व नैतिकता: राष्ट्र निर्माण की आधारशिला
जीवन में सफलता के लिए निरंतर सीखना जरूरी
राम के आदर्श: रामायण से जीवन सीखें और अपने आचरण में उतारें
बच्चे सीखें भगवान श्रीराम के जीवनादर्श | रामायण से नैतिक शिक्षा
नारी का सम्मान और सामाजिक योगदान
यक्ष और युधिष्ठिर का दिव्य संवाद
राम राज्य का दर्शन और आधार
सफलता की ओर साधना से रास्ता
सोने की सही दिशा कौनसी है? | उत्तर दिशा में सिर करके सोना क्यों वर्जित है?
कठिन समय में कौन साथ है?
माँ के अटूट प्रेम को सलाम
दो जून की रोटी - संघर्ष की कहानी
प्री-वेडिंग शूट: आधुनिकता की अंधी दौड़ या सांस्कृतिक पतन?
स्थानीय व्यापार का समर्थन करें
जीवन का असली उद्देश्य – सेवा, प्रेम और सद्भावना से जीवन जीना
चलते रहने का महत्व – कर्म, धैर्य और सकारात्मक सोच की ताकत
घोड़े पर योद्धा की मूर्तियों के संकेत: मुद्रा क्या दर्शाती है?
मानसिक शांति के लिए क्यों ज़रूरी है एक अच्छी दिनचर्या?
आलस्य और डर से बाहर निकलें: मानसिकता में बदलाव
क्या वास्तव में “बी प्रैक्टिकल” होना ज़रूरी है?
अपराध नियंत्रण में संस्कारों की भूमिका और सामाजिक सुधार
विनम्रता: व्यक्तित्व को निखारने वाला सबसे सुंदर मानवीय गुण
दीपोत्सव: भारतीय व्यापार, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा
राम से बड़ा राम का नाम
सफलता का फार्मूला: अभ्यास और जीवन मूल्य
पर्यावरण संकट बढ़ रहा है—अब बदलाव हमारी ज़िम्मेदारी है
अन्न का दुरुपयोग – दिखावे की संस्कृति में बर्बादी
किशोरों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियाँ
अयोध्या राम मंदिर का इतिहास और निर्माण
पहलगाम हमला: जब इंसानियत को धर्म से तोला गया
श्रम बिकता है, बोलो... खरीदोगे?
जीवन में सफलता के लिए धैर्य का महत्व
अहंकार का अंधकार | व्यक्तित्व और समाज पर प्रभाव
चलिष्याम निरंतर | जोखिम, परिवर्तन और सफलता का संबंध
रामायण महाभारत के युद्ध बनाम आधुनिक युद्ध
सच कहने का साहस है.. सलीका है कविता
सामाजिक संकट एवं सांस्कृतिक अवसाद की ओर बढ़ते भारतीय परिवार
चातुर्मास - सनातनी विज्ञान | पाँच तत्व, विज्ञान और परंपरा
मानवीय सद्गुण की आज बड़ी जरूरत | विनम्रता की शक्ति
जीवन में निर्णय का महत्व
तुलसीदास की दृष्टि में नारी शक्ति, प्रकृति, अग्नि और काल का दर्शन
प्रदूषण और निजी वाहनों का बढ़ता प्रभाव
सरकारी नियंत्रण से मन्दिरों को मुक्त करें – एक सनातनी पुकार
खिचड़ी: ढाई हजार साल पुराना भारतीय व्यंजन, स्वाद, परंपरा और इतिहास के साथ
भारत के शहरी क्षेत्रों में वाहन पार्किंग की चुनौतियाँ और समाधान
सहनशीलता का गिरता स्तर और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव | धैर्य और क्षमा का महत्व
कुंबकोणम के शक्ति मुत्तम मंदिर और गरीब पंडित की बगुला संदेश की कहानी
क्या हमारे कार्य करने की कोई सीमा होती है?
कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और अपनी असली क्षमता पहचानें
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – नारी शक्ति को सलाम
शब्द ही ब्रह्म है क्योंकि शब्दों से ही इस त्रिगुणात्मक संसार का सृजन संभव है
आंतरिक और बाहरी दुनिया — ध्यान से आत्म नियंत्रण की शक्ति
हेमू कालाणी – भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानी
नए वर्ष का स्वागत: सकारात्मक विचार, संकल्प और जीवन को खुशहाल बनाने वाले मंत्र
21वीं सदी: अवसर, चुनौतियाँ और डिजिटल युग में बाल मन का भविष्य
दर्शन क्या है? देखने और दर्शन के गहरे अंतर की आध्यात्मिक समझ
भक्ति का सच्चा अर्थ: मंदिरों से आगे, मानवता की ओर
क्षमा का मूल्य: भारतीय संस्कृति में क्षमाशीलता की परंपरा
अज्ञान से ज्ञान की ओर: वैदिक साहित्य में प्रकाश, सद्गुण और श्रेय मार्ग का संदेश
नारी: परिवार की कुशल प्रबंधक — भारतीय संस्कृति में नारी की शक्ति, भूमिका और महत्व
जीवन की बाँसुरी: सरलता से चुनौतियों को मधुर बनाने की कला
उत्तर भारत में पराली जलाना: किसानों और पर्यावरण के लिए स्थायी समाधान
पहली तूलिका, पहली कहानी: भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का अद्भुत संसार
रामचरितमानस में हास्य और व्यंग्य: तुलसीदास की अनोखी रचनात्मकता
भाषा का महत्व: मधुर वाणी, संस्कार और सभ्यता का वास्तविक परिचय
जीवन की बाँसुरी: कठिनाइयों को सरलता से जीतने की प्रेरणादायक सीख
हर विचार का आकर्षण
भारतीय नववर्ष क्यों मनाया जाता है??
डॉ. विक्रम साराभाई: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक
वीर बाल दिवस 26 दिसंबर | साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की अमर शहादत
माँ सरस्वती की आरती | विद्या की देवी
2026: समय की देहरी पर जागरण का वर्ष | चेतना, समाज और राष्ट्र पर विचार
मानव जीवन का दर्शन: धैर्य, समत्व और अनुभव की सनातन दृष्टि
अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय: आज की आवश्यकता | भारतीय दृष्टि
लोकतंत्र और भारतीय ज्ञान परंपरा | वैदिक जड़ें, संविधान और आधुनिक भारत
स्वामी दयानन्द सरस्वती: आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक और ऋषि
प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा एवं संस्कृत कथा साहित्य – दर्शन, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत
धर्म और कर्म का सच्चा अर्थ – कर्तव्य, निष्काम कर्म और जीवन का उद्देश्य
संवाद संस्कृति और बाल मनोविज्ञान – बच्चों को गलत निर्णय और आत्महत्या से कैसे बचाएं
बसंत ऋतु में होली – फागुन, प्रकृति और रंगों के उत्सव का मनोहारी वर्णन
लेखक के अन्य आलेख
बसंत ऋतु में होली – फागुन, प्रकृति और रंगों के उत्सव का मनोहारी वर्णन
धर्म और कर्म का सच्चा अर्थ – कर्तव्य, निष्काम कर्म और जीवन का उद्देश्य
लोकतंत्र और भारतीय ज्ञान परंपरा | वैदिक जड़ें, संविधान और आधुनिक भारत
वंदे मातरम्: राष्ट्रहित की आध्यात्मिक प्रेरणा | भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक
वीर बाल दिवस 26 दिसंबर | साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की अमर शहादत
रामचरितमानस में हास्य और व्यंग्य: तुलसीदास की अनोखी रचनात्मकता
उत्तर भारत में पराली जलाना: किसानों और पर्यावरण के लिए स्थायी समाधान
अज्ञान से ज्ञान की ओर: वैदिक साहित्य में प्रकाश, सद्गुण और श्रेय मार्ग का संदेश
भक्ति का सच्चा अर्थ: मंदिरों से आगे, मानवता की ओर
धनतेरस: समृद्धि का नहीं, संवेदना का उत्सव
शब्द ही ब्रह्म है क्योंकि शब्दों से ही इस त्रिगुणात्मक संसार का सृजन संभव है
कुंबकोणम के शक्ति मुत्तम मंदिर और गरीब पंडित की बगुला संदेश की कहानी
सहनशीलता का गिरता स्तर और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव | धैर्य और क्षमा का महत्व
भारत के शहरी क्षेत्रों में वाहन पार्किंग की चुनौतियाँ और समाधान
प्रदूषण और निजी वाहनों का बढ़ता प्रभाव
स्वास्थ्य के लिए आंसू क्यों ज़रूरी हैं
छला समर्पण | परिवार, संवेदना और अवमूल्यन की कथा
सच कहने का साहस है.. सलीका है कविता
चलिष्याम निरंतर | जोखिम, परिवर्तन और सफलता का संबंध
अहंकार का अंधकार | व्यक्तित्व और समाज पर प्रभाव
श्रम बिकता है, बोलो... खरीदोगे?
पहलगाम हमला: जब इंसानियत को धर्म से तोला गया
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से होने वाले खतरे
भारतीय परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक कारण
अपराध नियंत्रण में संस्कारों की भूमिका और सामाजिक सुधार
नवरात्रि में कोलू/गोलू: परंपरा और आधुनिकता का संगम
उत्तराखंड की 500 साल पुरानी परंपरा | सांस्कृतिक विरासत को सहेजती पहल
श्रावण मास में महादेव की आराधना: महत्व, व्रत और रस्में
चलते रहने का महत्व – कर्म, धैर्य और सकारात्मक सोच की ताकत
जाख अग्नि नृत्य – केदार घाटी की रहस्यमयी धार्मिक परंपरा
गर्मियों में खरबूजा खाने के फायदे
भारत के भोजन शैली और स्वाद की विविधता
चैत्र नवसंवत्सर 2025 का महत्व और उत्सव
जगदगुरु स्वामी माधवाश्रम जी | आध्यात्मिक जीवन और दर्शन
दक्षिण भारत में रक्षाबंधन का बदलता स्वरूप
विश्व नींद दिवस : डिसऑर्डर, सप्लीमेंट्स और स्वस्थ नींद के प्रभावी सुझाव
दुविधा – अनुभव और अस्वीकार्यता के बीच की दूरी
रावण की हड़ताल: दशहरा विशेष व्यंग्य
अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, पूजा विधि और 14 गांठों का रहस्य
शीतला सप्तमी व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व
राम – सत्य और धर्म का सार
सूर्य को जल अर्पण करना | सूर्य नमस्कार
प्रवासी भारतीय ही भारतीय संस्कृति के पहरेदार | नीदरलैंड में भारतीय संस्कृति का उजागर
असली रावण का अंत: जंगल की दशहरा कथा
पीपल की पूजा | भारतीय परंपरा में पीपल पूजा का वैज्ञानिक आधार
कुटुंब को जोड़ते व्रत और त्योहार – भारतीय परंपराओं का उत्सव
भूलते रिश्तों की चीख – एक भावनात्मक हिंदी लघुकथा
अक्षय नवमी: प्रकृति पूजन और आंवला वृक्ष की पूजा का पर्व | Akshaya Navami
एक पाती शिक्षक के नाम – शिक्षक की भूमिका और मूल्य आधारित शिक्षा
राष्ट्र का सजग प्रहरी और मार्गदृष्टा है, शिक्षक
नाश्ता: गरीबी, मानवीय रिश्तों और आत्मबोध की मार्मिक कहानी
लघुकथा : हार-जीत
सावन गीत
युग परिवर्तन
दर्द - भावनात्मक रूप
नारी और समाज
प्रेम की जीत
चाहत बस इतनी सी
आज का सबक - भारतीय परंपरा
देसी बीज
अलविदा मेरे प्यारे बेटे
भारतीय परम्परा की प्रथम वर्षगांठ
जीवन सार : प्रेरणादायक कहानी
शंखनाद
बड़ा लेखक
बच्चों के मन में अंकुरित विश्वास की सुंदर कहानी
यह घर बहुत हसीन है – एक भावनात्मक लघुकथा
मारबत - नागपुर का मारबत पर्व
पोला-पिठोरा (पोळा) - किसानों का प्रमुख त्योहार
तमाशा
ज्योतिष की विभिन्न विधाये और राजा सवाई जयसिंह (जयपुर) का योगदान
बसंत पंचमी माँ परमेश्वरी की जयंती | देवांगन समाज की कुल देवी
अच्युत, अनंत और गोविंद महिमा
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं | हनुमान जयंती